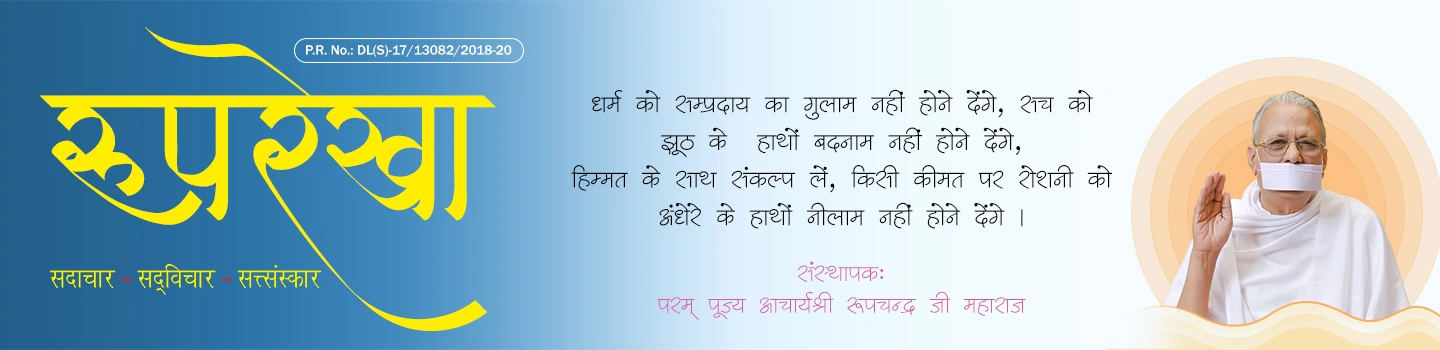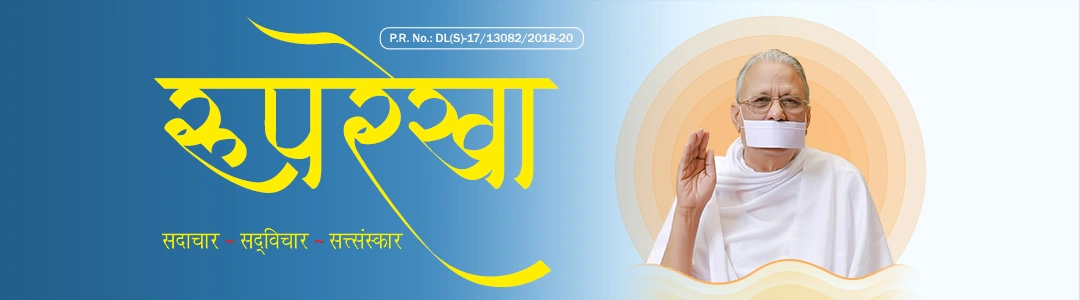अहिंसा की चर्चा के प्रसंग में मन में एक शब्द उगता है- मैत्री। इस शब्द से हम सब अच्छी तरह परिचित हैं, लेकिन इसके अर्थ से बहुत कम लोगों का परिचय होगा। हम मैत्री को भी एक संबंध के रूप में लेते हैं जबकि ऐसा है नहीं। संबंध का अर्थ है बांधना। मित्रता में भी साधारणतया हम एक-दूसरे को अपने से बांधते हैं। लेकिन हम यह भूल जाते है कि जो बांधा गया है, यह कभी खुल भी जाता है। यह जो स्थापित हुआ है, कभी विस्थापित भी हो सकता है। वह जो जोड़ा गया है, कभी टूट भी सकता है। साफ है कि अगर मैत्री को एक संबंध के रूप में समझेंगे तो उसके साथ ये सारे खतरे जुड़े रहेंगे। संबंध में सामूहिकता होने पर भी उसकी भाव-भूमि सार्वभौम नहीं होती है, क्योंकि बहुधा हर समूह में व्यक्ति खुद को अकेला पाता है। ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनमें सारा समूह अपने को पाता है और जो अपने को सारे समूह में पाते हैं। यह जो बाहर से जुड़ा हुआ है, भीतर से जुड़ा नहीं भी हो सकता है।
लेकिन जो भीतर से जुड़ा हुआ है, वह बाहर से जुड़ा न होने पर भी उससे अलग नहीं है। संबंध इसी कारण ऊपर से सुदृढ़ प्रतीत होते हुए भी टूट जाते हैं। सो, मैत्री अगर संबंध है तो सदा खतरे में है, लेकिन अगर वह संवेदना है तो उसके टूटने का प्रश्न ही नहीं है।
सच यह है कि मैत्री हमारा स्वभाव है। वह हमारा ‘होना’ है। ‘होना’ स्थिति है, न कि प्रक्रिया। ‘स्व’ प्रक्रिया का आरंभ है। जिसका आरंभ है उसका अंत भी सुनिश्चित है। स्थिति सनातन होती है। उसमें ‘स्व’ और ‘पर’ की पृथक सत्ताएं नहीं होती। सारी भेद-रेखाएं विभाव में दिखाई पड़ती हैं। स्वभाव तो अभेद और एकत्व से सतत संयुक्त है। वह जो हम नहीं है, उसी में हमारे होने के भ्रम से सारे भेद खड़े होते हैं। वहीं से सारे संघर्षों का जन्म होता है और अमैत्री का उद्भव होता है।
‘तुम’ और ‘वह’ समाप्त होकर जहां ‘मैं’ ही शेष रह जाता है, चेतना की वही स्थिति भावना के स्तर पर मैत्री, वृत्ति के स्तर पर अहिंसा और जीवन के सारे भौतिक-मानसिक स्तरों पर संयम के रूप में निष्पन्न होती है। उस परम चेतना की अनुभूति में न हम है, न तुम और न यह है, न कोई भी अन्य। मात्र समग्र है, सारे संदर्भों से मुक्त, सारी सीमाओं से परे। सीमा को जानना ही असीम में प्रवेश है। असीम में प्रवेश ही स्व का साक्षात्कार है, यही प्रेम है, मैत्री है। संबंध के रूप में किसी के समग्र है, सारे संदर्भों से मुक्त, सारी सीमाओं से परे। सीमा को जानना ही असीम में प्रवेश है। असीम में प्रवेश ही स्व का साक्षात्कार है, यही प्रेम है, मैत्री है। संबंध के रूप में किसी के साथ नहीं, लेकिन स्वभाव के रूप में। सर्वत्र सबके साथ।
मैत्री में किसी से जुड़ने की चेतना नहीं होती। इसलिए कि वहां अलगाव है ही नहीं। मैत्री हमारा वह आत्म-भाव है, जिसे न पाया जा सकता है और न खोया जा सकता है। न उसे बनाया जा सकता है, न मिटाया, जोड़ा या तोड़ा ही जा सकता है। मैत्री स्वयं के साथ स्वयं की महामयी चेतना है। खंडित एवं एकपक्षीय भाव नहीं। इस दृष्टि से मैत्री को जिस अर्थ में महावीर ने लिया है, उसका सार यह है कि उसे राग-द्वेष, आकर्षण-विकर्षण, सामीप्य एवं दूरी संबद्ध और असंबद्धता के द्वैत से पृथक करके देखना होगा। अपने में ही अपने प्रति मैत्री का स्रोत खोजना होगा। वह खोज लेंगे तो हम अपने और सबके मित्र होंगे अन्यथा किसी के कुछ भी नहीं हो पाएंगे।
-आचार्य रूपचन्द्र